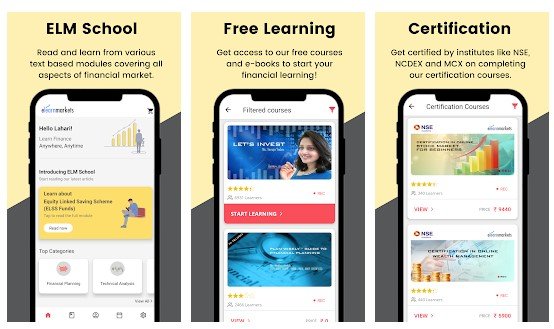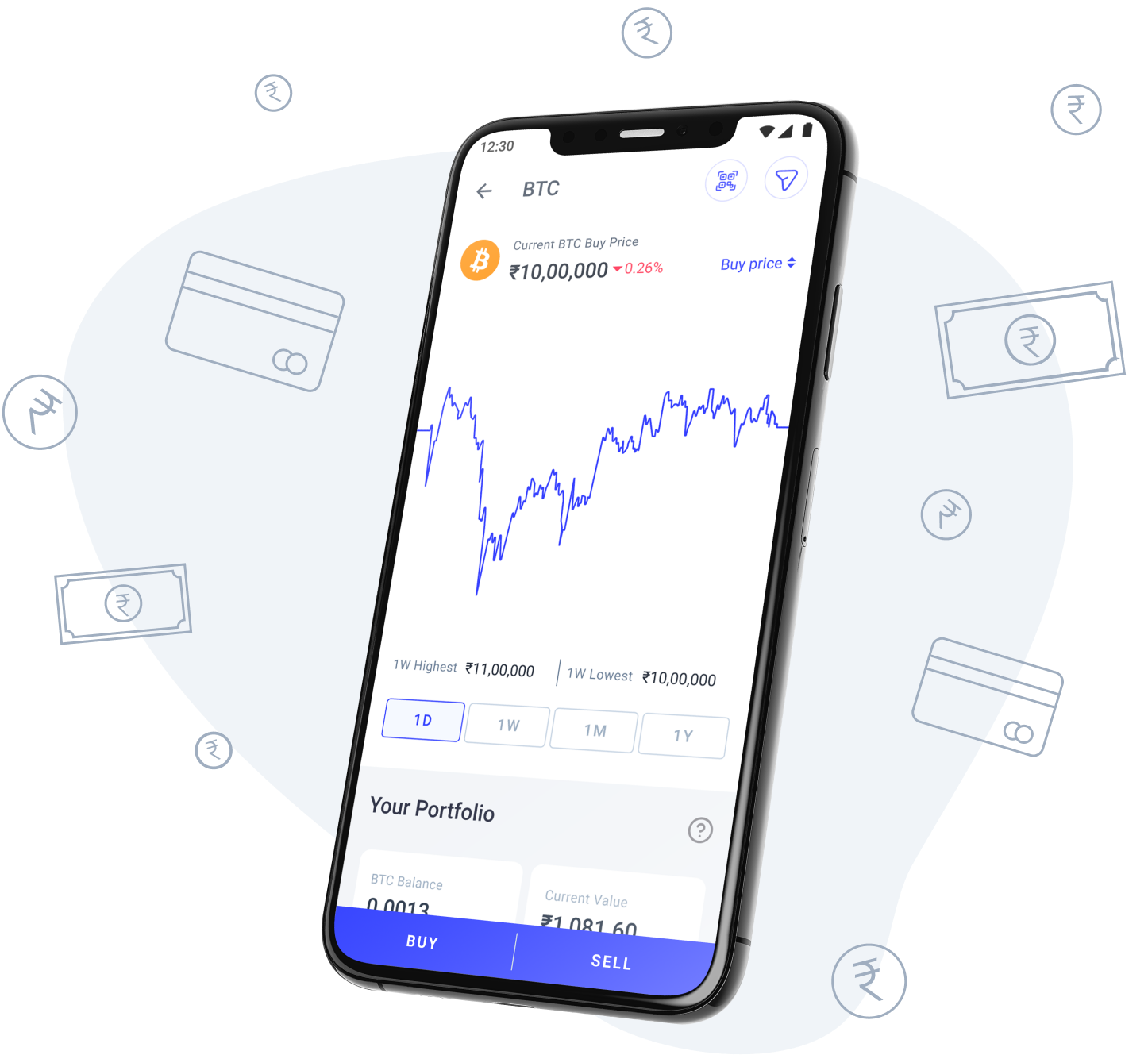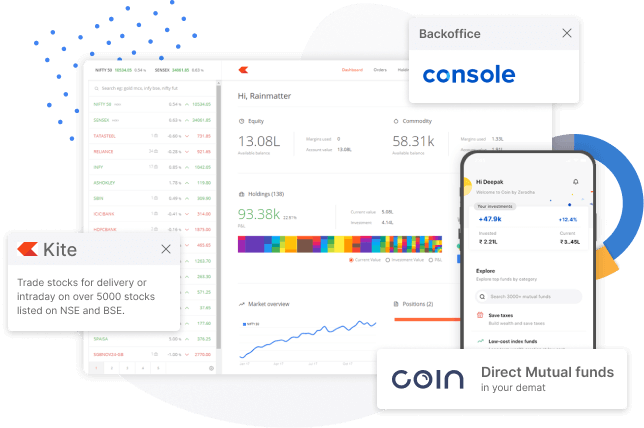#AjitAnjum #FarmsBill2020 #SinghuBorder
Farmer's Protest : इस किसान ने कानून की गजब व्याख्या कर दी Ajit Anjum
कृषि कानून, खेती का प्रश्न और वर्गीय दृष्टिकोण
विरोध में वर्चस्वकारी स्वर
हाल में कृषि क्षेत्र से संबंधित मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कानूनों पर तथाकथित हरित क्रांति के इलाकों के किसानों ने पिछले हफ्ते भर से दिल्ली के बार्डरों को जाम कर रखा है। ये आंदोलन इन इलाकों में सबसे प्रखर रहे हैं क्योंकि यहीं पर किसानों को सरकारी सहयोग से अधिक फायदा हुआ है। ये आंदोलन इन किसानों की व्याकुलता को दिखाता है। ये किसान कृषि के अंदर खुले बाजारीकरण की अनिश्चितताओं से घबराए हुए हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व अवश्य ही बड़े किसानों और उच्च मध्यम किसानों के हाथ मे है जिन्हें इस सहयोग से सबसे अधिक फायदा मिलता था।
ये भी सही है कि यह तबका बाजारीकरण के खिलाफ नहीं है। नियंत्रित बाजारीकरण और सरकारी संरक्षणवाद से अभ्यस्त होने के कारण, बिना किसी प्रकार के निर्धारित न्यूनतम सहयोग दाम की खुली बाज़ार व्यवस्था अवश्य ही इस तबके को असहज प्रतीत होती है। साथ ही उन्हें आभास है कि वित्तीय, व्यापारिक और औद्योगिक हितों को कृषि में खुली छूट ग्रामीण सामाजिक, आर्थिक और संपत्ति रिश्तों को इन हितों के अधीन कर देगा। इसीलिए ये किसान सरकारी सुरक्षा कवच मांग रहे हैं।
ये कानून संवैधानिक संघीय प्रणाली का उल्लंघन करते हैं। इस प्रणाली का ढहना धनी किसानों की क्षेत्रीय ग्रामीण सत्ता और राजनीति में दखल को निरस्त कर देगा। ये 1980-90 के दशक में स्थापित किसानों की राजनीतिक पहचान और शक्ति पर अंतिम वार है। पिछले तीन दशकों में बाजारोन्मुख कट्टरवाद ने भारत के सारे सार्वजनिक प्रणालियों और संस्थाओं को, जिनकी मदद से बाजार व्यवस्था की अराजकता को कुछ हद तक नियंत्रित किया जाता था, धीरे-धीरे कमजोर कर दिया है।
तमाम रंगों की सरकारों ने कमोबेश इस प्रक्रिया में योगदान किया है और साबित कर दिया है कि वे महज पूंजीवादी राजसत्ता के गिरगिटिय प्रकृति के अलग-अलग रंग हैं। विपक्षीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ और सरकारें नव-उदारवाद के दौर में सीधे बिचौलियों की भूमिका में आ गए हैं। पार्टियों के बीच समझ और चेहरों की जो भी पहचान हो राजसत्ता उन्हें सहज ही अपने सतरंगी चोले में जड़ लेती है। उनके लिए किसानों के निम्नपुंजीवादी क्षेत्रीय वर्गहित वित्तीयकृत पूंजी के बेरोक आवाजाही में रोड़ों की तरह लगते हैं। इसी कारण मुख्यधारा की पार्टियां कानूनों का विरोध नहीं कर रहीं, बस तात्कालिक समझौते द्वारा किसानों को शांत करने की बात कर रही हैं।
मौलिकता का प्रश्न
किसी भी सरकार की यही मंशा रहती है कि उसकी नीतियों को क्रांतिकारी अथवा मौलिक समझा जाए। क्योंकि इसी से वह अपने लिए एक विशिष्ट पहचान हासिल कर सकती है। 2014 के बाद से भारत में ऐसा ही कुछ हो रहा है।
मोदी सरकार अपनी सारी नीतियों को मौलिक बताती है। इसमें मीडिया का तो उसे पूर्ण सहयोग है ही, परंतु उससे भी अधिक विपक्षीय शक्तियां मोदी सरकार की मौलिकता को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़तीं। उनके अनुसार 2014 से भारत में कुछ मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं — नोटबंदी, जीएसटी, कश्मीर नीति, अमेरिका परस्ती, यूएपीए का भरपूर इस्तेमाल, एनआरसी-सीएए, और अब कृषि कानून!
तो निष्कर्षतः प्रशंसा और आलोचना का केंद्र भारत की पूंजीवादी व्यवस्था और उसकी राजसत्ता नहीं बल्कि तात्कालिक सरकार होती है।
ऐसा होने से तमाम आर्थिक और राजनीतिक संकटों की व्यवस्थागत नैसर्गिकता ओझल हो जाती है और सारा जन-आक्रोश महज तात्कालिक सरकार के खिलाफ सीमित हो जाता है। इसी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था और राजतंत्र की निरंतरता बनी रहती है।
कांग्रेस ने जिस प्रक्रिया की शुरुआत की थी भाजपा उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रही है। अगर ध्यान दें तो तीनों कृषि कानूनों पर काम मनमोहन सिंह सरकार के वक्त पूरा हो चुका था और सरकारी मंडियों को कमजोर करने का काम भी लगातार दो दशकों से खुले तौर पर हो रहा था। कई राज्य सरकारों ने कानूनी बदलाव कर दिए थे। परंतु जरूरत थी इन सारे बदलावों को देश के स्तर पर संघटित कर कृषि बाजार व्यवस्था को एकीकृत करने की। इसके लिए जिस तरह के अधिनायकत्व की जरूरत है वह केवल मोदी नेतृत्व में भाजपा और आरएसएस का संगठित बहुसंख्यकवाद ही प्रदान कर सकता है।
इस संदर्भ में एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि मोदी सरकार ने कभी भी अपनी घोर नव-बनिकवादी (उत्पादन से अधिक ख़रीद-बिक्री, सट्टाबाज़ार आधारित और बड़े व्यापारियों व साहूकारों के हाथों में सम्पत्ति और आर्थिक सत्ता को केंद्रित करने की) मंशाओं को नहीं छुपाया। नव-बनिकवाद और नव-उदारवाद का मिश्रण जो वैश्विक स्तर पर दक्षिण पंथ के रूप में हम आज उभरता देख रहे हैं उसका भारतीय प्रस्तुतिकरण है मोदी सरकार।
आर्थिक गतिविधियों के तमाम स्वरूपों को वित्तीयकृत और केंद्रीकृत कर वाणिज्यिक और औद्योगिक सत्ता समूहों के धंधों के साथ जोड़ना, यही इसका मुख्य काम रहा है। छोटे, मंझोले और स्थानीय धंधों को वर्चस्वकारी औपचारिक पूंजी व्यवस्था के साथ जोड़ कर उनकी स्वायत्तता को पूंजी की सत्ता के अधीन श्रम नियोजन के विभिन्न और विशिष्ट स्वरूपों के तौर में तब्दील कर देना यही तो मोदी सरकार के तमाम आर्थिक “सर्जिकल” हमलों का मतलब रहा है।
तीन कृषि कानूनों को भी इसी रूप में समझा जाना चाहिए। एक ही झटके में मोदी सरकार की कोशिश है कि वित्तीय पूँजी के नेतृत्व में कृषि और उद्योग के नव-उदारवादी समन्वय के लिए वैधानिक आधार तैयार हो जाए।
आखिर इन कानूनों में क्या है?
किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून, 2020
यह कानून कृषि उपजों के विक्रय के लिए सरकारी मंडियों के एकाधिकार को समाप्त करता है। उसका मानना है कि इससे विकल्प आधारित बाजार व्यवस्था का विकास होगा और वैकल्पिक बाजारों व व्यापार के लिए आधारिक संरचना हेतु निवेश का अन्तर्वाह होगा।
पिछले दो दशकों से कृषि उत्पाद के व्यापार की व्यवस्था में वैधानिक स्तर पर सुधार करने की कोशिश हो रही है ताकि कृषि सप्लाई चेन में प्रतिस्पर्धा तेज हो सके, और कृषकों को वैकल्पिक व्यापार चैनलों द्वारा अपने उत्पाद के लिए उचित दाम प्राप्त हो सके। परंतु अलग अलग राज्यों ने इन सुधारों को एकरूपता के साथ नहीं लागू किया है।
नीति-निर्माताओं के लिए कानूनी स्तर पर एकरूपता की कमी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य वातावरण और आधुनिक व्यापार व्यवस्था के विकास को बाधित करती है। इस कानून द्वारा कृषि उपजों के अंतर-राज्यीय मुक्त बाजार बनाने की कोशिश है।
इस कानून के कारणों में कृषि को लेकर सरकार की समझ साफ है – वह केवल खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करती बल्कि कृषि-उद्योग के लिए कच्चा माल भी मुहैया कराती है । इसीलिए कृषकों अर्थात कृषि को सीधे इन कृषि-उद्योगों से जोड़ना सप्लाई चेन को छोटा करेगा और व्यापार-लागत और कटाई के बाद के घाटे को कम करेगा। निरंतर बदलते कृषि-वातावरण, ई-व्यापार और कृषि-निर्यात के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए सरकारी व्यवस्था से बाहर सुलभ और प्रतिस्पर्धी व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता है।
कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020
पहला कानून जहां कृषि मंडियों को पूंजीवादी बाजार नियमों के अनुरूप व्यवस्थित कर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक ही सूत्र में बांधने की कोशिश करता है, तो यह कानून कृषि संबंधों में औपचारिकता और एकरूपता लाकर उन्हें वित्तीय और औद्योगिक पूंजी के साथ सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह कानून कृषि से जुड़े करारों के लिए राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करने का दावा करता है जिनके द्वारा किसान कृषि सेवाओं और भविष्य के कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए कृषि-उद्यम कंपनियों, प्रोसेसरों, होलसेलरों, आयातकर्ताओं और बड़े व्यापारियों के साथ करार कर सकता है। कृषि सेवाओं के अंतर्गत कुछ विशिष्ट कार्य उल्लेखित हैं —बीज, चारा, कृषि रसायन, मशीनरी और प्रौद्योगिकी, सलाह, गैर रसायनिक कृषि-सामग्री और इस तरह के अन्य सामग्रियों की आपूर्ति।
इस कानून के पक्ष में दलील यह है कि भारतीय कृषि की विशिष्ट कमजोरियां हैं। छोटे भूमि जोत के कारण वह विखंडित है। साथ ही मौसम पर निर्भरता, उत्पादन और व्यापारिक अनिश्चितता कई कमजोरियों से भारतीय कृषि ग्रसित है। ये कमजोरियां कृषि में निवेश और उत्पादन के प्रबंधनों दोनों को ही जोखिम भरा और प्रभावहीन बना देता है। अधिक उत्पादकता, किफायती उत्पादन और उत्पाद के प्रभावी मौद्रीकरण के लिए इन कमजोरियों से लड़ना होगा। कानून के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए करारों के प्रोत्साहन से शायद मौद्रीकरण की प्रक्रिया मजबूत होगी जिसका प्रमुख उद्देश्य है कई स्तरों पर कृषि से जोखिम हटाना, अधिक मूल्यों वाले कृषि उत्पादो के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए उद्योग द्वारा निवेश की बढ़ोत्तरी, आयात के लिए प्रोत्साहन और कार्यकारी कुशलता।
आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020
इस संशोधन द्वारा प्रमुख खाद्य सामग्रियों —अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल — के दामों पर सरकारी नियंत्रण हटा दिया गया है। यही नहीं यह कानून ऐसी व्यवस्था तैयार करता है जिससे भविष्य में क्षेत्रीय सरकारों के लिए इन सामग्रियों के विक्रय पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाना लगभग असंभव हो जाएगा।
आंदोलन और सामाजिक असंतोष
यह साफ़ है कि ये क़ानून ग्रामीण जीवन की क्षेत्रीयता को और उसके साथ ग्रामीण (निम्न)पूँजीवादी शक्तियों को वित्तीय नेटवर्क के पूरक इकाइयों में तब्दील कर देते हैं। बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक हितों के महज़ आपूर्तिकर्ताओं के रूप में ही उनकी पहचान बच जाती है। शायद कुछेक बड़े पूँजीपति कृषक कृषि-उद्योग की दुनिया में अपनी जगह कॉंट्रैक्टरों के रूप में बना पाएँ परंतु बाक़ियों को अपने श्रम, भूमि और अन्य श्रम-साधनों को इन हितों के अधीनस्थ ही करना होगा। इस आंदोलन में यही आशंका साफ़ दिखती है। और इसीलिए इसको 1980 के दशक के किसान आंदोलन से जोड़ना ठीक नहीं है। उस समय सवाल बाज़ार में अपने लिए साख बनाने का था, जबकि आज यह अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले तीन दशकों की राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं ने कृषि को जिस अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है उसका नतीजा है यह।
अवश्य ही इस आंदोलन का नेतृत्व जो मूलतः अमीर और उच्च मध्यम किसानों का है उसके लिए मुद्दा मोल-भाव का है परंतु आंदोलन केवल नेतृत्व, उनकी भाषा और प्रमुख नारे नहीं होते। ये तत्व अवश्य ही उनकी पहचान बनाते हैं, और उन्हीं के आधार पर व्यवस्था भी आंदोलनों से बातचीत करती है। परंतु कोई भी आंदोलन इतना ही नहीं होता, उसको व्यवस्था के प्रतिनिधित्वकारी तर्क में बांधना उसके सामाजिक संदर्भ से हटाकर महज रूपवादिता और वैधानिकता में समेटना होगा। किसी ने सही ही बताया है आंदोलन सामाजिक असंतोष का जलागम क्षेत्र होता है —अपने समय और स्थान के कई प्रकार के असन्तोष आंदोलन के उभार में शामिल होते हैं। चल रहे किसान आंदोलन को केवल उसके वर्चस्वकारी नेतृत्व और नारे के आधार पर समझना बेमानी है। मझोले, छोटे किसानों और अन्य अर्ध-गँवई आबादी की भागीदारी को उनकी नासमझी बताना तथा आंदोलन को एकीकृत करके देखना हिरावलवादी लिलिपुटियों की आपसी बौद्धिक जुगाली है।
किसी भी आंदोलन की द्वंद्वात्मक व्याख्या उसके अंतर्विरोधों को उजागर कर अंतर्निहित संभावनाओं को प्रदर्शित करना है। यह संभव है कि किसी आंदोलन का विद्यमान स्वरूप अपने आप में परिवर्तनकारी और दूरगामी न हो परन्तु उसके अंदर ही नई आंदोलनकारी संभावनाओं की बीज भी होती है —और उस बीज की पहचान ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों के आधार पर की गई टिप्पणियों से अवश्य ही नहीं हो सकती। ठोस स्थिति के ठोस मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। विडंबना यह है कि वामपंथ का सबसे बड़ा तबक़ा आज फ़ासीवाद की लड़ाई के नाम पर ऐसा संयुक्त मोर्चा रचने में लगा है जिसमें वर्गीय प्रश्न बिलकुल ही ग़ायब है और यह वामपंथ राजनीतिक विपक्षवाद के अंदर बिचौलियों की भूमिका अदा कर रहा है। परंतु गरमदलीय वामपंथ का भी बड़ा हिस्सा अस्तित्ववादी राजनीतिक तात्कालिकवाद में फँसा है और सारे आंदोलनों को तत्काल राहत के रूप में देखता है। साथ ही उसे अभी भी भारत में स्थानिक पूँजीवाद की कमी खलती है और मोदी की नीतियों में भी कुछ सामंती-साम्राज्यवादी-क्रोनी-पूँजीवाद दिखता है और इसीलिए वह किसानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक पूँजीवादी शक्ति का आधार-वर्ग देखता है। इस कारण उसे किसानों के आंतरिक विभेदन के आधार पर राजनीति ग़लत लगती है।
दूसरी तरफ़ हिरावलवादी लिलिपुटियन दस्तों का मजदूरवाद वर्ग को प्रक्रिया नहीं पहचान के रूप में देखता है और उसे पूँजीवाद की सड़ीगली बर्बर अवस्था में भी पवित्र मजदूर के अवतरण का इंतज़ार है। उसे मोदी के कृषि क़ानूनों में शायद उसकी झलक दिख गई है। परंतु “पूँजी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती की कि श्रम का प्राविधिक स्वरूप कैसा है। वह जैसा भी होता है, पूँजी उसी को लेकर अपना काम आरम्भ कर देती है।” और आज जब नव-उदार त्वरित वित्तीयकरण द्वारा तमाम मूर्त श्रम-प्रक्रियाओं का तात्कालिक अमूर्तीकरण सम्भव है तो उसको किसी भी प्राविधिक स्वरूपों को तब तक बदलने की ज़रूरत नहीं जब तक वह बाधा न हो जाए। इसीलिए हमारे हिरावलवादियों का पवित्रता का सपना स्वप्निल ही रह जाएगा।
किसान नहीं बेशीकृत आबादी का आंदोलन – श्रम का कृषि प्रश्न
भारत और अन्य “विलंबित” पूँजीवादी देशों में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र केवल कृषि उत्पादों के उत्पादन का क्षेत्र नहीं है। वह ख़ास तौर से इन देशों में पूँजीवाद का सबसे अहम पण्य — श्रम शक्ति — का नर्सरी भी है, जिसके आधार पर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएँ निवेशकों के लिए आकर्षक होती हैं। ये क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा के अभाव में भारत की अपार बेशी आबादी का पालना है — सस्ते श्रम का कारण है। आँकड़े बताते हैं कि अधिकाधिक कृषक परिवार ऐसे हैं जो महज खेती से अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकते। यही नहीं पूंजीवाद में सामाजिक आवश्यकताओं का डायनामिक्स ऐसा होता है कि संभ्रांत दिखने वाले कृषक तबके की भी खेती अधिकाधिक गैर-कृषि व्यवसायों की भरपाई करने वाले व्यवसाय का रूप लेती चली जाती है।
नवउदारवादी श्रम प्रबंधन के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रमिक असुरक्षित अनियमित रोजगार ही हासिल कर पाते हैं। उनके लिए गांव, खेती अथवा छोटे स्व-रोज़गार का अवसर अपनी, पारिवारिक और भविष्य की श्रम-शक्ति के उत्पादन और पुनरुत्पादन के लिए अनिवार्य है — इसीलिए स्व-रोजगार को छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं। कृषि और अन्य कृषि-संबंधित व्यवसाय से बड़ा स्व-रोजगार का साधन कहाँ है? इसीलिए अफ्रीका और लैटिन-अमरीका के कई मार्क्सवादियों और कार्यकर्ताओं ने आज के संदर्भ में कृषि/भूमि प्रश्न को पुनर्परिभाषित करने की बात कही है। पूंजीवादी विकास की आरंभिक अवस्था मे भूमि/कृषि प्रश्न पूंजी संचय और उत्पादकता की आवश्यकता से जुड़ा था। भूमि सुधार का संघर्ष परजीवी लगानकारी हितों को हटाकर पूंजी निवेश की समस्या से जुड़ा था। आज भूमि/कृषि प्रश्न श्रम के प्रश्न के रूप में उभर रहे हैं —वे श्रमिकों के जिंदा रहने से जुड़े हैं। इसके विपरीत “कृषि पूंजीवाद” में खेती का प्रश्न गौण होकर कृषि-व्यवसाय/ उद्योग ही केंद्र में हो गया है, जो कि इन तीनों कानूनों में साफ दिखता है।
“रोजगार पाने की अनिश्चितता और अनियमितता, बार-बार श्रम की मंडी में मजदूरों का आधिक्य हो जाना और इस स्थिति का बहुत देर तक बने रहना” — यही तो बेशी आबादी के लक्षण हैं। पंजाब के सरकारी आँकड़ों के अनुसार युवा बेरोजगारी दर लगभग 21 प्रतिशत है। इसके अलावे कितने हैं जो बेरोजगारी की अवस्था में कृषि या अन्य स्व-रोजगार पर निर्भर हो जाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में ऐसे कई युवक मिल जाएंगे जो रोजगार की तलाश में हैं पर पारिवारिक कृषि पर निर्भर हैं। कृषि बेशीकृत आबादी को जिंदा रखता है।
भारत में शहरी मजदूरों की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों से सम्बद्ध है, नव-उदारवादी श्रम नियोजन के तहत अस्थाई रोजगार में बढ़ोत्तरी इस संबंध को मिटने नहीं देता। इस तबके के लिए कृषि उत्पाद मजदूरी की कमी की भरपाई का साधन होता है। आज के दौर में अधिकाधिक किसानों के सीमांतीकरण ने किसानी का मतलब ही बदल दिया है —वे आज सही मायने में अव्यक्त अथवा प्रच्छन्न बेशी आबादी के हिस्से के रूप में मजदूरों की रिज़र्व सेना में शामिल हो गए हैं। आज खेती का प्रश्न महज इसी बेशीकृत आबादी का प्रश्न है। खेती करने और बचाने की लड़ाई इस तबके के लिए कोई मुनाफे और बाजारी सहूलियत की लड़ाई नही है, बल्कि “रोजगार पाने की अनिश्चितता और अनियमितता” के संदर्भ में जिंदा रहकर श्रम-शक्ति के पुनरुत्पादन की लड़ाई है।
चल रहे आंदोलन में भी इस वर्गीय अंतर्विरोध को हम देख सकते हैं। अवश्य ही नेतृत्वकारी बयानों और नारों में यह व्यक्त नहीं हो सकता। मजदूर वर्गीय दृष्टिकोण से इसी अन्तर्विरोध को समझने, उच्चारित करने, तेज करने और इसके आधार पर किसानी के क्षेत्र में वर्ग संगठन के विकास में सहयोग देने की जरूरत है। यही दृष्टिकोण सही मायने में पूंजीवाद-विरोधी कृषि के सामाजिक स्वरूप के विकास के लिए जमीन तैयार करेगा —पूंजी-आधारित खेती के खिलाफ आवश्यकता-केंद्रित उत्पादन प्रक्रिया की नींव रखेगा।
आइये हम अपनी बात का अंत भारत के महान किसान नेता और मार्क्सवादी स्वामी सहजानंद सरस्वती के एक उद्धरण से करें:
सच पूछिए तो अर्द्धसर्वहारा खेत–मज़दूर ही, जिनके पास या तो कुछ भी ज़मीन नहीं है या बहुत ही थोड़ी है और टुटपुँजिए खेतिहर, जो अपनी ज़मीन से किसी तरह काम चलाते और गुजर–बसर करते हैं, यही दो दल हैं, जिन्हें हम किसान मानते हैं, जिनकी सेवा करने के लिए हम परेशान और लालायित हैं औरअन्तततोगत्वा वही लोग किसान–सभा बनाएँगे, उन्हें ही ऐसा करना होगा।
तब 1940 का दशक था…
लोकपक्ष पत्रिका दिसम्बर 2020,